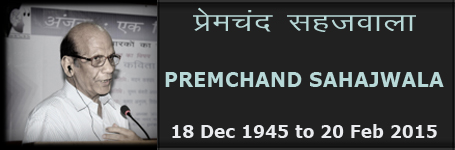सन् 70-80 के दशक में मैं सोनीपत में तैनात था व खूब कहानियां लिखता था. तभी एक दिन एक मित्र ने आ कर बताया कि दिल्ली में मन्नू भंडारी की कहानी ‘यही सच है’ पर आधारित एक फिल्म चल रही है ‘रजनीगन्धा’. ‘रजनीगन्धा’ देख कर मैं चकित था और लगा था कि कहानी अब कागज़ से उड़ कर पर्दे पर आ गई है. पर इस से भी ज़्यादा प्रभावित मैं तब हुआ जब मैंने श्याम बेनेगल की फिल्में ‘अंकुर’ व ‘मंडी’ देखी. इसके बाद देखी गोविन्द निहालानी की ‘अर्ध-सत्य’. मेरे लिये सचमुच यह चमत्कार सा था कि कहानियों की जिन प्रवृत्तियों को हम इतना अधिक विश्लेषित कर के उन्हें ‘नई कहानी’ या ‘साठोत्तरी कहानी’ जैसी संज्ञाएं देते हैं, वे सब के सब रचना तत्व ज्यों के त्यों पर्दे पर फ़िल्मी विधा के रूप में भी मौजूद है. फिल्म ‘अर्ध-सत्य’, ‘अंकुर’ व ‘मंडी में तो मुझे नई कहानी का बिम्ब विधान भी नज़र आ गया और इस के बाद मैं इस सामानांतर कहे जाने वाले सिनेमा का दीवाना सा हो गया. मैंने ‘स्पर्श’, ‘पार’, ‘अंकुश’, ‘सुबह’, ‘निशांत’ आदि कई फिल्में देखी. पर जिस फिल्म ने मेरे मन पर एक प्रकार से जीवन भर का प्रभाव डाला वह थी शबाना आज़मी–मार्क जुबेर-दीप्ति नवल द्वारा अभिनीत फिल्म ‘कमला’. ‘कमला’ फिल्म वैसे तो एक वास्तविक घटना पर आधारित थी जिसमें ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ के संवाददाता अश्विनी ने भारत के किसी इलाके से एक लड़की खरीदी और उस समय के पत्रकारिता जगत में यह साबित कर के तहलका मचा दिया कि आज भी भारत में लड़कियां खरीदी और बेची जाती हैं. पर फिल्म बनाते समय उसके पत्रकार मार्क जुबेर को एक महत्वाकांक्षी पत्रकार दिखाया गया जो किसी दूरस्थ इलाके से एक लड़की ‘कमला’ (दीप्ति नवल) खरीद लाता है और उसे अपने कैरियर का मोहरा बनाना चाहता है. पर फिल्म के मध्यांतर से पहले के आखिरी दृश्य में अचानक खरीदी हुई लड़की ‘कमला’ मार्क जुबेर की पत्नी शबाना आज़मी से पूछ बैठती है – ‘तुम को कितने में खरीद कियो?’ शबाना का मुंह फटा का फटा ही रह जाता है और वही स्थिति हॉल में बैठे असंख्य दर्शकों की हो जाती है. फिर मध्यांतर के बाद शुरू होती है उस महत्वाकांक्षी पत्रकार की पत्नी शबाना आज़मी की दर्दीली कहानी. अपने चरम तक आते आते फिल्म यह साबित कर चुकी होती है कि ‘कमला’ सिर्फ वह नहीं है जो पैसे दे कर खरीदी या बेची जाती है बल्कि भारतीय समाज में तो हर ‘कमला’ हर मोड़ पर मिल जाएगी, एक खरीदी हुई बांदी की तरह. पुरुष प्रधान समाज में शोषित नारी की तस्वीर दिखने वाली शायद इस से अधिक सशक्त फिल्म कोई न हो. नारी हर जगह ‘कमला’ की तरह खरीदी हुई बांदी की तरह है. एक दृश्य में शबाना तड़प कर मार्क से कहती है – ‘नहीं नहीं मैं कमला हूँ… तुमने मुझे खरीद रखा है मैं कमला हूँ…’ फिल्म में वे सांकेतिक दृश्य बहुत प्रभावशाली हैं जिनमें एक पत्नी के रूप में शबाना केवल पति के कामों में लगी रहती है, उसी का कोट हैंगर से उतार कर सही जगह लगा रही है, उसी का फोन अटेंड करती है. समाज में उसकी पहचान केवल एक मिसेज़ खन्ना के रूप में है. ऐसा महत्वाकांक्षी बुद्धिजीवी व्यक्ति पत्नी को केवल इस्तेमाल करने की एक वस्तु स समझता है और जब उसे सेक्स की ज़रूरत महसूस होती है तभी वह उसके शोषण के तौर पर उसके सामने अपनी डिमांड रखता है. कहानी में एक आदर्शवादी पत्रकार ए.के.हंगल भी है जो जुबेर से पूछता है – ‘भई किसी अखबार में लिखा है तुमने ‘कमला’ को दो सौ में खरीदा किसी में लिखा है ढाई सौ में..’ तब मार्क जुबेर गुरूर से कहता है – ‘आप सही जानकारी के लिये हमारे अखबार पढ़िए न!’ फिल्म के प्रारंभ में जब उस दूरस्थ इलाके में जुबेर ‘कमला’ को खरीद कर अपनी गाड़ी में बैठता है तब ‘कमला’ उस गाड़ी में नहीं बैठती वरन अपनी गठरी संभाले किसी बंधे हुए डोर सी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ती नज़र आती है. जब वह पत्रकार के घर आ जाती है तब उसके प्रति पत्रकार की तटस्थता देखने योग्य है. किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह ‘कमला’ घर में सोफे पर नहीं बैठती या घर के मेम्बर की तरह का कोई दर्जा उसे नहीं मिलता, वरन वह तो ज़मीन पर उकडू बैठी भिखारिन सी इधर इधर फटकती रहती है और जब जुबेर पहली बार अपने पत्रकार समूह के सामने उसे कार में लाता है तब उस का पत्रकार दोस्त अनु मलिक कार के बाहर उसका मखौल सा उड़ाता गाने लगता है:
कमला रानी बाहर आओ / बाहर आ कर दरस दिखाओ..
खरीदी हुई लड़की के प्रति ऐसा वितृष्णात्मक नजरिया हो या बीबी को इस्तेमाल करने वाली एक वास्तु समझने का नज़रिया, ‘कमला’ फिल्म हर दृष्टि से एक बेहद सशक्त फिल्म बन पड़ी जिस में ‘साठोत्तरी कहानी’ की तरह पात्र अपनी परिस्थियों के विरुद्ध एक मोर्चा स बांधे खड़े हैं, भले ही वे हार जाएँ. आज जब ‘तारे ज़मीन पर’ और ‘पीपली लाईव’ जैसी सशक्त फिल्में देखने को मिलती हैं, जिनमें समाज के वास्तविक पात्र हैं और जीवन के सामानांतर चलती कहानियां हैं तो उस ज़माने की यादें सहज ही आ जाना स्वाभाविक है. हिंदी सिनेमा हिंसा और ग्लैमर की दुनिया में भटकता हुआ इन असली फिल्मों से किस कदर वंचित रहा, यह इन् तमाम फिल्मों को देख कर सहज ही समझा जा सकता है. काश ‘रजनीगन्धा’ ‘अर्धसत्य’ ‘कमला’ व ‘सुबह’ जैसी फिल्में नियमित रूप से आज भी, इस बदले हुए तकनीक और माहौल में बनें. कम से कम समाज को सोचने वाला और प्रबुद्ध बनाने के लिये यह एक स्वस्थ बात होगी
Wednesday, December 29, 2010